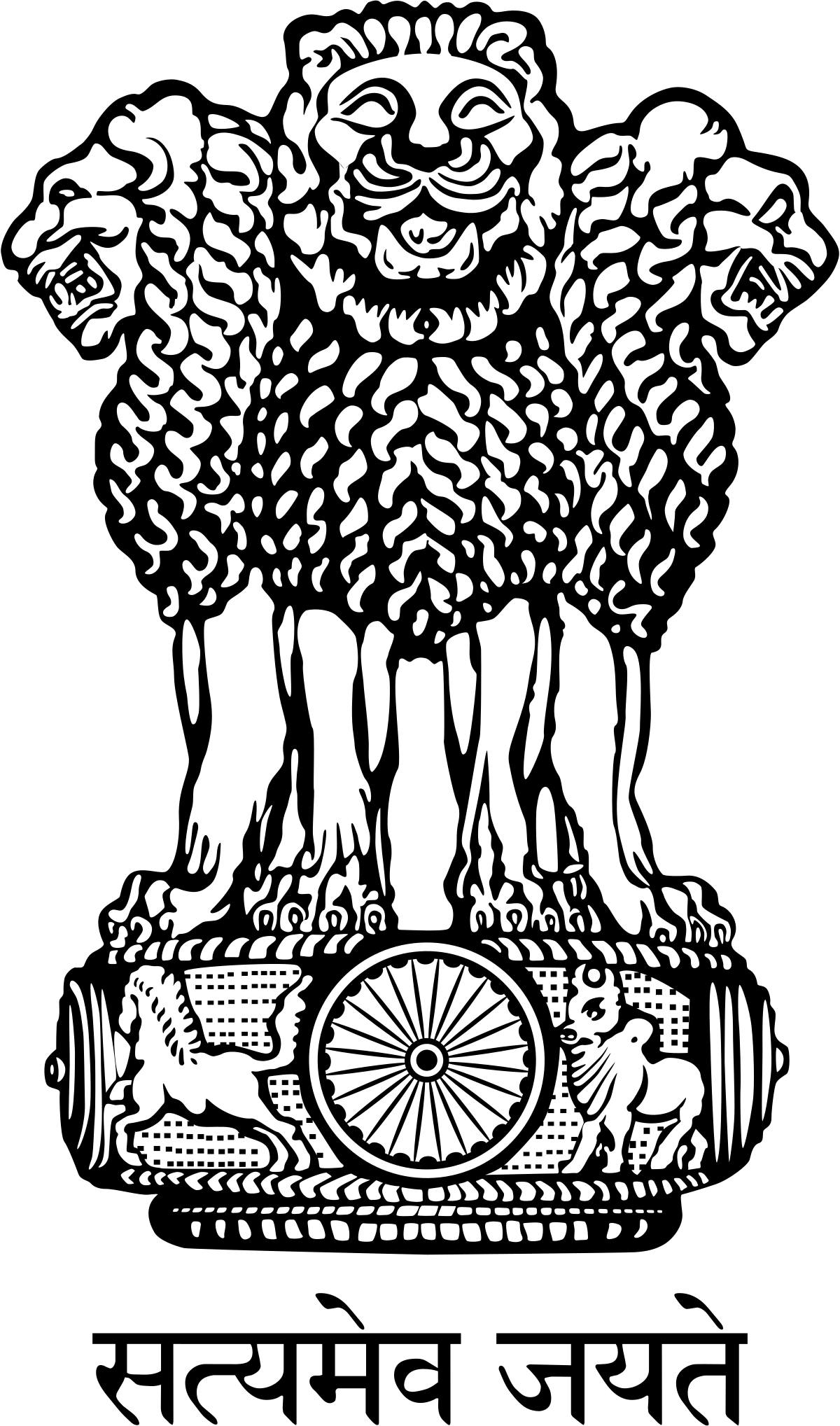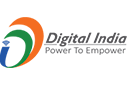SPEECH OF PUNJAB GOVERNOR AND ADMINISTRATOR, UT CHANDIGARH, SHRI GULAB CHAND KATARIA ON THE OCCASION OF NATIONAL AGRICULTURE WORKSHOP ON THE OCCASION OF WORLD BEE DAY AT MOHALI ON MAY 20, 2025.
- by Admin
- 2025-05-20 21:50
‘विश्व मधुमक्खी दिवस’ के अवसर पर
राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का संबोधन
दिनांकः 20.05.2025, मंगलवार समयः दोपहर 12:00 बजे स्थानः मोहाली
नमस्कार!
आज विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव कर रहा हूँ।
यह दिन न केवल प्रकृति की अद्भुत रचना, मधुमक्खियों के महत्व को उजागर करता है, बल्कि इसके माध्यम से हम प्रकृति, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र में उनके अद्भुत योगदान को भी समझने का अवसर प्राप्त करते हैं।
विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है, जो स्लोवेनिया के महान मधुमक्खी पालक एंटोन जान्सा की जयंती है। इसका उद्देश्य है लोगों को मधुमक्खियों के संरक्षण, उनके महत्व और उनसे जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूक करना।
इस वर्ष की थीम, ‘‘प्रकृति से प्रेरित हों ताकि हम सभी का पोषण हो’’, मधुमक्खियों की हमारे कृषि खाद्य प्रणाली एवं जैव विविधता को बनाए रखने में उनकी केन्द्रीय भूमिका का स्मरण कराती है।
देवियो और सज्जनो,
भारत में मधुमक्खी पालन केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक बन चुका है।
यह न केवल फसलों की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि करता है, बल्कि जैव विविधता को बनाए रखने, पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करने और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में भी प्रभावी भूमिका निभाता है।
पंजाब, जो कि देश का अग्रणी कृषि राज्य है, ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मधुमक्खी पालन को अपनाकर इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यहाँ के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ-साथ मधुमक्खी पालन को एक लाभकारी सह-उद्योग के रूप में विकसित कर रहे हैं।
पंजाब में शहद उत्पादन के साथ-साथ वैल्यू एडेड उत्पादों जैसे मधुमक्खी का मोम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और पराग संग्रहण जैसे उप-उद्योगों में भी सक्रियता देखी जा रही है। यह परिवर्तन किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बना रहा है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहा है।
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हम ‘हनी एंड एपिकल्चर डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ (HADAI)’ के उद्घाटन के साथ सहयोग, नवाचार और सतत विकास के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं।
यह संस्था न केवल मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कार्यरत किसानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों को एक साझा मंच प्रदान करेगी, बल्कि प्रशिक्षण, अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन और नीति-निर्माण के क्षेत्र में एक प्रभावशाली सहयोगी की भूमिका भी निभाएगी।
संस्था का उद्देश्य है कि देशभर के मधुमक्खी पालकों को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे वे अपने उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि कर सकें।
यह मंच मधुमक्खी पालन से संबंधित चुनौतियों को चिन्हित कर उनके समाधान हेतु ठोस रणनीतियाँ विकसित करेगा और किसानों को बाजार से सीधा जोड़ने में भी मदद करेगा।
इस पहल से न केवल ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों के निर्यात को भी नया बल मिलेगा। HADAI के माध्यम से भारत वैश्विक शहद उद्योग में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है।
मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में ‘राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड’ का पुनर्गठन किया गया था।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल फसलों की उत्पादकता में परागण के माध्यम से वृद्धि करना है, बल्कि शहद और मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाकर किसानों और मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि करना भी है।
यह बोर्ड प्रशिक्षण, अनुसंधान, गुणवत्ता मानकों और नीति निर्माण के जरिए इस क्षेत्र को एक संगठित एवं लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
देवियो और सज्जनो,
हमारे युवाओं को मधुमक्खी पालन को केवल पारंपरिक कृषि गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावनाओं से परिपूर्ण, टिकाऊ और सम्मानजनक आजीविका के रूप में देखने के लिए प्रेरित करना समय की महती आवश्यकता है।
मधुमक्खी पालन में आधुनिक तकनीकों का समावेश, जैसे एपिथैरेपी (मधुमक्खी उत्पादों से उपचार), एपी-पर्यटन (Bee Tourism)] कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हाइव मॉनिटरिंग, और ट्रैसेबिलिटी सिस्टम इस क्षेत्र को अत्याधुनिक और उच्च मूल्य वाला उद्यम बना सकते हैं।
इन तकनीकों के माध्यम से न केवल उत्पादन की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, यह नवाचार युवाओं को स्टार्टअप की भावना के साथ मधुमक्खी पालन जैसे परंपरागत क्षेत्र में उतरने के लिए प्रेरित करता है।
ऐसे प्रयास न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यापक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेंगे।
देवियो और सज्जनो,
मधुमक्खियाँ केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं हैं। वे परागण (Pollination) की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करती हैं, जो हमारी कृषि प्रणाली की रीढ़ है।
आज मधुमक्खियाँ और अन्य परागण करने वाले जीव जैसे कि तितलियाँ, चमगादड़ और हमिंगबर्ड्स मानव गतिविधियों के कारण दिन-ब-दिन गंभीर खतरे में पड़ते जा रहे हैं। यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि परागण प्रकृति की उन बुनियादी प्रक्रियाओं में से एक है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतरता और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।
विश्व के लगभग 90 प्रतिशत जंगली फूलों की प्रजातियाँ पूरी तरह या आंशिक रूप से, जीवों द्वारा किए जाने वाले परागण पर निर्भर करती हैं। इतना ही नहीं, 75 प्रतिशत से अधिक खाद्य फसलें और 35 प्रतिशत वैश्विक कृषि भूमि परागण पर निर्भर हैं।
यह बात अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि परागणकर्ता जीव न केवल खाद्य सुरक्षा को सीधा सहयोग प्रदान करते हैं, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण में भी इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
दुनिया में 2 लाख से अधिक जीव-जंतुओं की प्रजातियाँ परागणकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। इनमें से अधिकांश तितलियाँ, पक्षी और चमगादड़ सहित 20 हजार से अधिक प्रकार की मधुमक्खियों जैसे वन्य जीव हैं।
मधुमक्खियाँ और अन्य परागणकर्ता पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संवेदनशील संकेतक भी हैं। ये हमें पारिस्थितिकी तंत्र की दशा और जलवायु परिवर्तनों की ओर संकेत देते हैं। इनके संरक्षण से न केवल जैव विविधता को बल मिलता है, बल्कि मृदा की उर्वरता, कीट नियंत्रण, जल और वायु शुद्धता जैसी पारिस्थितिक सेवाओं में भी सुधार होता है।
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे कृषि अभ्यासों को अपनाएँ जो प्रकृति के अनुकूल हों, जैसे कि एग्रोइकोलॉजी, इंटरक्रॉपिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री और एकीकृत कीट प्रबंधन। ये पद्धतियाँ परागणकर्ताओं को संरक्षण देती हैं, जिससे फसल की पैदावार स्थिर बनी रहती है, खाद्य संकट को कम किया जा सकता है, और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सकता है।
जब हम परागणकर्ताओं के संरक्षण हेतु सुनियोजित प्रयास करते हैं, तो हम जैव विविधता के अन्य घटकों का भी संरक्षण करते हैं। इससे हमारी पारिस्थितिकी और कृषि प्रणाली दोनों सशक्त बनती हैं।
परागणकर्ताओं के महत्व, उनके सामने मौजूद खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को ‘विश्व मधुमक्खी दिवस’ के रूप में घोषित किया है।
इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं की रक्षा हेतु ठोस कदम उठाना है, जिससे वैश्विक खाद्य आपूर्ति की समस्याओं को सुलझाने और विकासशील देशों में भूख की चुनौती को कम करने में भी सहायता मिलेगी।
हम सभी पर परागणकर्ताओं के संरक्षण की जिम्मेदारी है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उनके घटते अस्तित्व की निगरानी करें और जैव विविधता की क्षति को रोकने के लिए मिलकर प्रयास करें।
इसके लिए हमें सबसे पहले, मधुमक्खियों के लिए सुरक्षित कीटनाशक प्रोटोकॉल को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। अनियंत्रित और विषैले कीटनाशकों का प्रयोग मधुमक्खियों के जीवन चक्र पर गंभीर प्रभाव डालता है। इसके स्थान पर हमें जैविक और पर्यावरण-मित्र कीटनाशकों को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा किसानों को इन तकनीकों के प्रशिक्षण देने चाहिए।
दूसरा, पुष्प गलियारों (Floral Corridors) का विकास अत्यंत आवश्यक है। ऐसे गलियारे, जो विविध मौसमी पुष्पों से युक्त हों, मधुमक्खियों को वर्षभर पराग और अमृत की निरंतर आपूर्ति प्रदान करते हैं। ये गलियारे कृषि क्षेत्रों, सड़क किनारों और ग्राम्य क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं।
तीसरा, हमें जलवायु-लचीली और उच्च गुणवत्ता वाली मधुमक्खी प्रजातियों के विकास की दिशा में अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण मधुमक्खियों की पारंपरिक नस्लें संकट में हैं। इसके लिए अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों को मिलकर काम करना होगा।
चौथा, इस अभियान की सफलता हेतु जन-जागरूकता आवश्यक है। विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं से ही बच्चों को पर्यावरण और मधुमक्खियों की उपयोगिता के विषय में शिक्षित किया जाए। साथ ही पंचायत स्तर पर किसानों और उपभोक्ताओं के बीच भी लगातार संवाद व जागरूकता अभियान चलाए जाएँ ताकि यह विषय केवल वैज्ञानिक विमर्श तक सीमित न रहे, बल्कि एक जनांदोलन का रूप ले।
इस संदर्भ में मैं यह सुझाव देता हूँ कि पंजाब को भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र और उत्तराखंड के पंतनगर की तर्ज पर एक अत्याधुनिक राज्य स्तरीय एपिकल्चर केंद्र की स्थापना करनी चाहिए।
इस केंद्र में विभिन्न प्रकार के मधुमक्खी-प्रेमी पुष्पों के विशाल बागान विकसित किए जाएँ। यह केंद्र एक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का केंद्र बने, जिसे उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाए।
यह केंद्र न केवल किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा, बल्कि युवाओं को भी मधुमक्खी पालन को एक आधुनिक, लाभदायक एवं सम्मानजनक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इससे न केवल प्रदेश की कृषि आय में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा।
इस अवसर पर मैं, विशेष रूप से युवाओं, छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वे मधुमक्खियों से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा दें और नवाचार के माध्यम से इस क्षेत्र में नई संभावनाएँ तलाशें।
अंत में, मैं सभी किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और मधुमक्खी पालन से जुड़े उद्यमियों का आभार प्रकट करता हूँ जो इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।
आइए, इस ‘विश्व मधुमक्खी दिवस’ पर हम यह संकल्प लें कि हम मधुमक्खियों जैसे प्रकृति के अद्भुत उपहार के संरक्षण में अपना योगदान देंगे और एक संतुलित, सुरक्षित तथा समृद्ध पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
धन्यवाद,
जय हिंद!