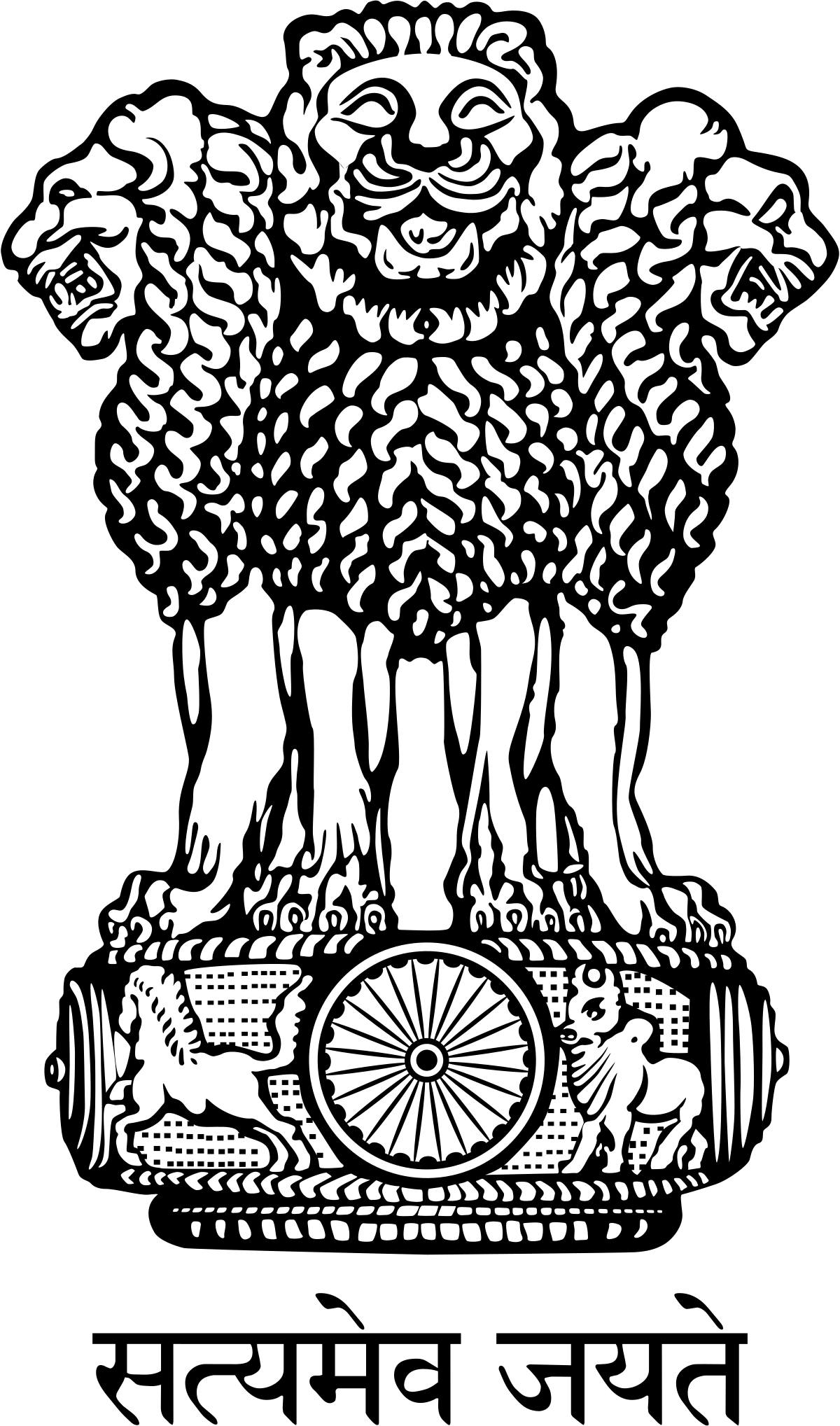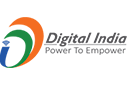Speech of Punjab Governor and Administrator, UT, Chandigarh, Shri Gulab Chand Kataria on the occasion of Eid Milan celebrations at Chandigarh on May 21, 2025.
- by Admin
- 2025-05-22 09:00
‘ईद मिलन समारोह’ के अवसर पर
राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का संबोधन
दिनांकः 21.05.2025, बुधवार
समयः शाम 6:15 बजे
स्थानः चंडीगढ़
नमस्कार!
आप सभी को ईद-उल-फितर अथवा ईद की दिली मुबारकबाद। आज का यह अवसर न केवल उल्लास और भाईचारे का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक सौहार्द, साझा मूल्यों और एकता की भावना को भी मजबूत करता है।
ईद मिलन का उत्सव ईद-उल-फितर और ईद-उल-जूहा के दरमियान मनाया जाता है।
ईद साल में दो बार मनाई जाती है, पहली ईद रमजान के रोजों की समाप्ति के अगले दिन मनाई जाती है जिसे ईद-उल-फितर कहा जाता है और दूसरी ईद-उद-जूहा है।
रमजान का महत्व यह है कि इस महीने कुरआन शरीफ अवतरित हुआ था। कुरआन जिसमें सारी मानवता की भलाई निहित है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 31 मार्च को देशभर में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में फैले मुस्लिम समुदाय द्वारा ‘ईद-उल-फितर’ या ‘ईद’ का पर्व बड़े ही श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया।
हम सभी जानते हैं कि ईद-उल-फितर इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जो रमज़ान के पवित्र महीने के समापन पर मनाया जाता है। यह पर्व आत्मसंयम, त्याग, करुणा और सेवा की भावना को समर्पित है।
रोज़ा रखने से व्यक्ति के भीतर आत्म-संयम की भावना विकसित होती है, मन पवित्र होता है और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति उत्पन्न होती है। यह आत्मिक अनुशासन, संयम और आत्मविश्लेषण का माध्यम बनता है।
ईद के दिन लोग अल्लाह से अपने पापों की माफी मांगते हैं और अपने लिए तथा अपने प्रियजनों के लिए अमन, सलामती और बरकत की दुआ करते हैं। यह दिन आत्मिक शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक होता है।
‘ईद-उल-फितर’ में ‘फितर’ का अर्थ है, धर्मार्थ उपहार। इस्लाम में इसे ईद का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। नमाज से पूर्व हर संपन्न मुसलमान के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह निर्धनों और ज़रूरतमंदों को ‘फितर’ अर्पित करे, ताकि वे भी ईद की खुशियों में सम्मिलित हो सकें। यह परंपरा समता, उदारता और सामाजिक न्याय का सशक्त संदेश देती है।
रमज़ान का महीना आत्मचिंतन, संयम और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक होता है, और ईद-उल-फितर इस तपस्या की पूर्ति का उत्सव है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तभी सच्चा आनंद प्राप्त होता है।
साथियो,
चैरिटी, यानी दान या परोपकार, हर धर्म की मूल आत्मा है। यह न केवल किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने का माध्यम है, बल्कि आत्मिक उन्नति और सामाजिक समरसता का भी आधार है।
हिंदू धर्म में कहा गया है, ‘‘परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्’’, अर्थात परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप। भारतीय संस्कृति में गंगा, वायु, वृक्ष, सूर्य, सभी प्राकृतिक तत्व बिना किसी भेदभाव के परहित के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए प्रकृति को भी हम गुरू, माता और ईश्वर के समान मानते हैं।
सिख धर्म में गुरुओं ने परोपकार को परम कर्तव्य बताया है। ‘‘गरीब दा मुंह, गुरु की गोलक’’ अर्थात जो गरीब है, उसका पेट भरना, उसकी मदद करना, स्वयं ईश्वर को अर्पण करने के समान है। यह संदेश सेवा और समर्पण की महान परंपरा को दर्शाता है, जिसे सिख पंथ ने अपने जीवन का मूल बना लिया है।
इस्लाम धर्म में भी कुरान की आयतें बार-बार यह उपदेश देती हैं कि इंसान को उदार और क्षमाशील होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद साहब ने यह शिक्षा दी कि जो लोग साधन-संपन्न हैं, वे केवल अपने लिए नहीं जी सकते; उनका नैतिक दायित्व है कि वे गरीबों, असहायों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। यदि उनके पास संपत्ति है, लेकिन उनके आसपास कोई भूखा या बेसहारा है, तो वह दौलत निरर्थक है।
ईद का पर्व इस परंपरा और भावना का जीवंत प्रतीक है। यह केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता, परमार्थ, दान और परस्पर सौहार्द का पर्व है।
खुदा की सच्ची इबादत तभी मानी जाती है, जब उसके बनाए बंदों की सेवा की जाए। ज़कात और फित्रा जैसे धार्मिक आदेश इस्लाम में इसीलिए हैं ताकि समाज में आर्थिक संतुलन बना रहे और हर व्यक्ति ईद की खुशियों में शामिल हो सके।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहते थे, ‘‘मानवता का धर्म ही सच्चा धर्म है और मानव सेवा ही ईश्वर की सबसे सच्ची सेवा है।’’ इसी भावना से प्रेरित होकर यदि हम समाज में एक-दूसरे का सहारा बनें, तो यही ईद का सच्चा संदेश और उद्देश्य होगा।
देवियो और सज्जनो,
भारतवर्ष एक बहुधर्मी, बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देश है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है, अनेकता में एकता। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सहित अनेक धर्मों के लोग सह-अस्तित्व की भावना के साथ रहते हैं।
हर क्षेत्र, हर प्रांत, हर समुदाय की अपनी अलग भाषा, परंपराएं, रीति-रिवाज और जीवनशैली है, फिर भी सब एक साझा राष्ट्रीय भावना से जुड़े हुए हैं।
भारत की यह विशेषता इसे विश्व के अन्य देशों से अलग बनाती है। यहाँ उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भले ही पहनावे, खान-पान और बोलियाँ अलग हों, लेकिन सभी के दिलों में बसता है एक ही भारत, हमारा भारत।
पर्व-त्योहारों में भागीदारी, संकट के समय एकजुटता, और एक-दूसरे की संस्कृति का सम्मान, यही वे सूत्र हैं जो भारत की एकता को मजबूती प्रदान करते हैं।
हमारी यह विविधता न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करती है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की भी बुनियाद है। अतः यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस अद्भुत विविधता को सम्मान दें, उसकी रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे एक जीवंत उदाहरण के रूप में संरक्षित रखें।
साथियो,
दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं के लिए अपेक्षा करते हैं। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल दूसरों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता विकसित करते हैं, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में भी प्रेरित करता है।
यह सोच हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने, उनके अनुभवों और संघर्षों को सम्मान देने की शिक्षा देती है। इस प्रकार हम दूसरों की पीड़ा को महसूस कर पाते हैं और सहयोग एवं सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। यही भावना समाज में एकता, विश्वास और आपसी सद्भाव को जन्म देती है।
प्रेम, करुणा और क्षमा, ये तीन तत्व मानवता की आत्मा हैं। इनके बिना समाज केवल एक बेजान ढांचा बनकर रह जाता है। प्रेम हमें जोड़ता है, करुणा हमें प्रेरित करती है, और क्षमा हमें आत्मिक शांति प्रदान करती है। जब कोई समाज इन मूल्यों को अपनाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में सभ्य, समावेशी और समरस बनता है।
हमारा भारतवर्ष इन मूल्यों का प्राचीन वाहक रहा है। यहाँ का मूल दर्शन रहा है, “वसुधैव कुटुम्बकम्”, जिसका अर्थ है “सारी पृथ्वी एक परिवार है”। यह दृष्टिकोण सीमाओं, धर्मों, जातियों और भाषाओं से परे जाकर एक सार्वभौमिक एकता की बात करता है। यह विचार हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति का दुःख केवल उसका निजी विषय नहीं है, बल्कि वह पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
इसलिए, जब हम ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना को आत्मसात करते हैं, तो हमारे व्यवहार में सेवा, दया, क्षमा, और समानता जैसे गुण स्वतः आ जाते हैं। यह हमें जात-पात, ऊँच-नीच, धर्म या वर्ग की सीमाओं को पार कर एक व्यापक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है।
आज के समय में, जब दुनिया अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही है, तब यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम इन मूल्यों को फिर से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दूसरों के प्रति वही व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं, यही आत्मीयता, यही सह-अस्तित्व और यही सच्ची मानवता है।
आज का यह ईद मिलन समारोह हमें यह अवसर देता है कि हम एक-दूसरे की भावनाओं को समझें, एक-दूसरे की परंपराओं का सम्मान करें, और एकजुट समाज की दिशा में काम करें। एक ऐसे समाज की परिकल्पना करें जहाँ कोई भेदभाव न हो, जहाँ हर नागरिक को समान अवसर मिले और जहाँ सभी धर्मों के लोग मिल-जुलकर भारत की प्रगति में योगदान करें।
मैं इस अवसर पर सभी नागरिकों से यह अपील करता हूँ कि वे एकता, शांति और भाईचारे के इस संदेश को केवल अपने घरों तक सीमित न रखें, बल्कि अपने मोहल्लों, गाँवों और शहरों में भी फैलाएँ। आइए हम मिलकर नफरत और विभाजन की दीवारों को गिराकर प्यार और विश्वास की पुलों का निर्माण करें।
यह भी याद रखें कि ईद केवल मिठास और उत्सव का पर्व नहीं है, यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। ज़कात और फितरा जैसे प्रावधान इसी भावना को दर्शाते हैं। इसलिए, इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम समाज में सबके कल्याण और न्याय के लिए कार्य करें।
अंत में, मैं एक बार फिर आप सभी को ईद की ढेरों शुभकामनाएँ देता हूँ। यह पर्व आपके जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति लेकर आए।
धन्यवाद,
जय हिंद!