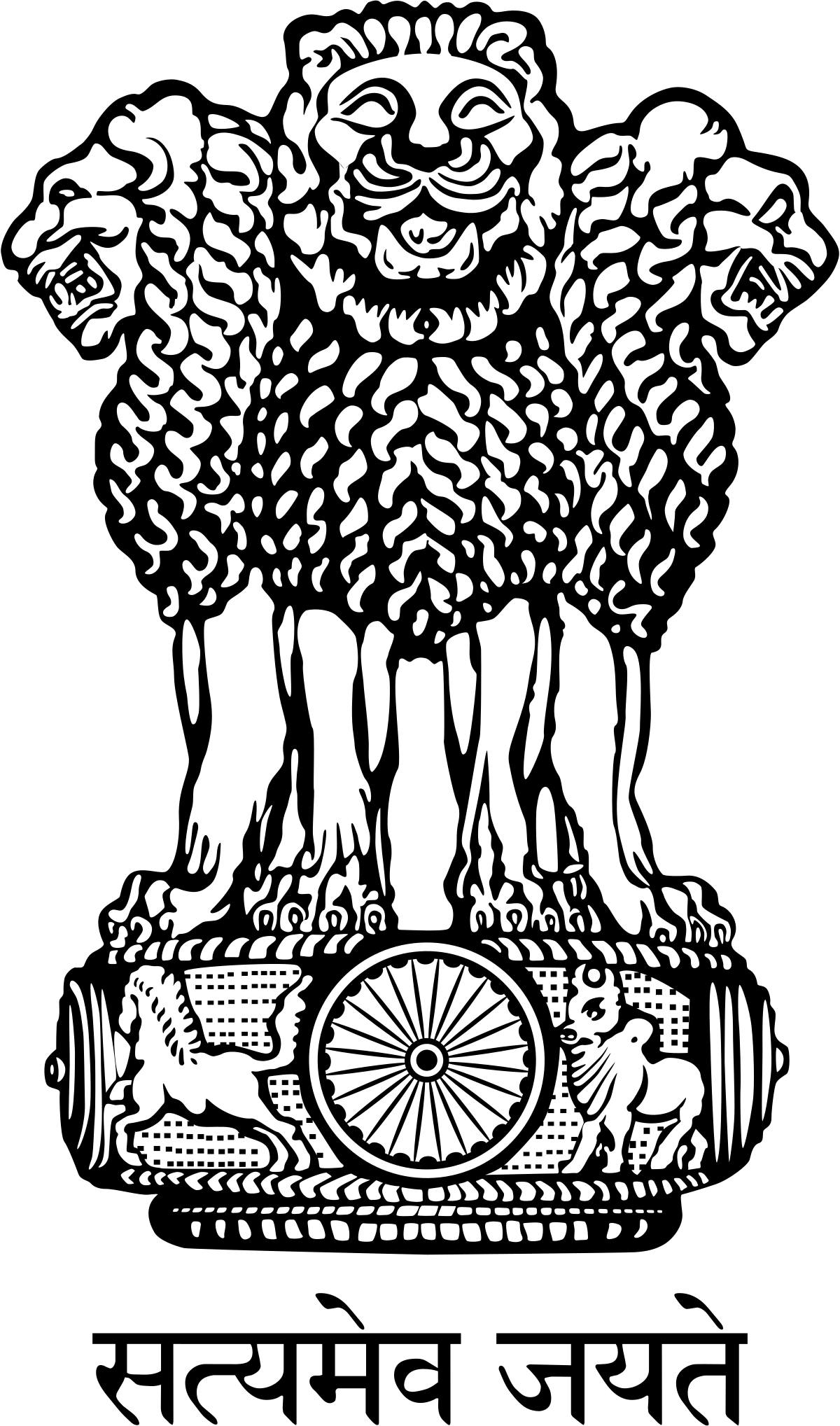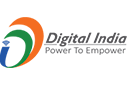SPEECH OF PUNJAB GOVERNOR AND ADMINISTRATOR, UT CHANDIGARH, SHRI GULAB CHAND KATARIA ON THE OCCASION OF INTERACTIVE SESSION WITH TEACHERS AT CHANDIGARH ON SEPTEMBER 26, 2025.
- by Admin
- 2025-09-29 18:35
‘संयुक्त शिक्षक संघ’ द्वारा आयोजित शिक्षक दिवस पर
राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का संबोधन
दिनांकः 26.09.2025, शुक्रवार समयः शाम 4:45 बजे स्थानः चंडीगढ़
नमस्कार!
आज मुझे ‘संयुक्त शिक्षक संघ’ द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले, मैं देश के सभी शिक्षकों को नमन करता हूँ और आप सबको इस विशेष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।
मुझे बताया गया है कि संयुक्त शिक्षक संघ की स्थापना 21 अप्रैल 2023 को हुई थी। इसकी स्थापना प्रमुख समाजसेवी तथा शिक्षक श्री रणवीर जी द्वारा की गई, जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं और इसका सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं।
संगठन में पंजाब, हरियाणा, समग्र शिक्षा अथॉरिटी तथा यूटी कैडर के लगभग 3 हजार शिक्षक सदस्य हैं। संगठन का उद्देश्य केवल शिक्षकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा समाज के उत्थान में भी सक्रिय योगदान देना है।
जानकर प्रसन्नता हुई कि यह संगठन केवल शिक्षा क्षेत्र तक सीमित न रहते हुए समाज की समस्याओं में भी योगदान देता है। हाल ही में इसने पंजाब के बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान कर मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर जनहित कार्यों में सहभागिता कर संगठन अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निभा रहा है।
इसकी कार्यप्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है और शिक्षकों की सामूहिक शक्ति का प्रयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। संगठन की मूल सोच ‘शिक्षक से समाज तक’ है, जिसका अर्थ है कि केवल शिक्षक हित ही नहीं, बल्कि विद्यार्थी और समाज के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
देवियो और सज्जनो,
हम सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस हमारे महान दार्शनिक, विद्वान, शिक्षक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि शिक्षा केवल ज्ञान पाने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण का सबसे बड़ा साधन है।
हम सभी जानते हैं कि शिक्षक वह दीपक हैं, जो स्वयं जलकर समाज और राष्ट्र के भविष्य को आलोकित करते हैं। आप शिक्षक न केवल पढ़ाते हैं, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन में मूल्य, संस्कार और दिशा भी प्रदान करते हैं। आपके समर्पण और परिश्रम से ही हमारे विद्यालय और महाविद्यालय नई ऊँचाइयों को प्राप्त करते हैं।
भारतीय संस्कृति में गुरू को ईश्वर के तुल्य माना गया है। यही कारण है कि हमारे विचारक सदैव कहते आए हैं कि शिक्षक केवल ज्ञानदाता नहीं, बल्कि राष्ट्र के चरित्र निर्माता होते हैं। जैसा आचरण गुरु का होगा, वैसा ही शिष्य बनेगा, “यथा आचारः तथा अनुचरः।
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कहते थे, “A teacher has to create a lifelong autonomous learner" अर्थात शिक्षक का लक्ष्य ऐसा विद्यार्थी तैयार करना होना चाहिए जो जीवनभर सीखता रहे, अपनी क्षमताओं का विस्तार करता रहे और आगे चलकर समाज का सुधारक और राष्ट्र का निर्माता बने।
शिक्षक का सबसे बड़ा पुरस्कार कोई पद, सम्मान या सरकारी पुरस्कार नहीं है, बल्कि उसका वह विद्यार्थी है जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर अपने गुरु का नाम गौरवान्वित करता है। यही कारण है कि शिक्षण को एक पवित्र तपस्या माना जाता है।
महापुरुषों ने कहा है कि यदि किसी राष्ट्र को कमजोर या बर्बाद करना हो, तो उसकी शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दो। क्योंकि शिक्षा ही वह आधारशिला है, जिस पर किसी समाज और राष्ट्र का भविष्य निर्मित होता है। यदि शिक्षा संस्कारयुक्त और मूल्याधारित है, तो वही राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने की क्षमता रखती है।
किसी ने ठीक ही कहा है, "Knowledge is Power", अर्थात् ज्ञान ही वास्तविक शक्ति है। यह शक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि सीखने, अनुभव करने और समझ विकसित करने से आती है। ज्ञान से हम कठिन परिस्थितियों का समाधान खोज सकते हैं, समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने साथ-साथ देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, “ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं।”
देवियो और सज्जनो,
हमारी शिक्षा व्यवस्था आज कई अवसरों और चुनौतियों के बीच खड़ी है। सबसे पहली चुनौती है समान अवसर की। गाँव और शहर, निजी और सरकारी विद्यालयों और डिजिटल और पारंपरिक शिक्षा के बीच गहरी खाई हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या व ढाँचागत सुविधाएँ कम हैं और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, जबकि शहरी व निजी स्कूलों में आधुनिक तकनीक, प्रयोगशालाएँ और स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध हैं।
डिजिटल युग में यह असमानता और बढ़ गई है। संपन्न परिवारों के बच्चे ई-लर्निंग और ए.आई. साधनों से लाभान्वित हैं, जबकि गरीब तबकों के बच्चों को सामान्य इंटरनेट और उपकरण भी नहीं मिल पाते।
इसे दूर करने के लिए सरकार, समाज और निजी क्षेत्र को मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, डिजिटल ढाँचा मजबूत करना होगा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देना होगा, ताकि हर बच्चा समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सके।
दूसरी चुनौती है गुणवत्ता। शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न केवल पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान और परीक्षा के अंकों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्ची शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में सोचने, विश्लेषण करने और रचनात्मकता की शक्ति को विकसित करना है। यदि पढ़ाई केवल रटने और अंक प्राप्त करने का माध्यम रह जाएगी तो विद्यार्थी वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं हो पाएँगे।
गुणवत्ता का अर्थ है ऐसी शिक्षा, जो विद्यार्थियों में जिज्ञासा और समस्या-समाधान की क्षमता जगाए, उन्हें नए विचारों को स्वीकार करने और स्वयं नए विचार प्रस्तुत करने का साहस दे। इसके लिए कक्षाओं में संवाद आधारित शिक्षा, प्रोजेक्ट वर्क, प्रयोगशालाओं में शोध और डिजिटल टूल्स का उपयोग बढ़ाना होगा।
साथ ही, शिक्षकों को भी पारंपरिक ढर्रे से आगे बढ़कर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, तर्क करने और अपने विचार रखने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ऐसी शिक्षा ही युवाओं को न केवल रोजगार के लिए तैयार करेगी, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, नवाचारी और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला नागरिक बनाएगी।
तीसरी चुनौती है मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव। तेज़ जीवनशैली और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने शिक्षा को प्रायः केवल रोजगार और आर्थिक सफलता तक सीमित कर दिया है, जिससे नैतिकता, अनुशासन, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल जीवन-मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं।
सच्ची शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक या नौकरी नहीं, बल्कि जिम्मेदार, संवेदनशील और नैतिक दृष्टि वाला नागरिक बनाना है। इसलिए विद्यालयों को पाठ्यक्रम के साथ चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, सामाजिक सेवा और संस्कारों के विकास पर बल देना होगा।
शिक्षक अपने आचरण और अनुशासन से विद्यार्थियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। खेल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, योग, सामुदायिक सेवा और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम बच्चों में नैतिक मूल्यों को मजबूत कर उन्हें जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करने योग्य बनाते हैं। यही मूल्य आधारित शिक्षा उन्हें केवल नौकरी योग्य नहीं, बल्कि संतुलित, सफल और समाज को दिशा देने वाला सच्चा नागरिक बनाती है।
चौथी चुनौती की बात करूं तो अब तकनीकी परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था को गहराई से रूपांतरित कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में केवल पारंपरिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है; विद्यार्थियों को बदलते रोजगार बाजार, नवाचार और उद्यमशीलता के कौशल सीखने होंगे।
शिक्षकों को अब डिजिटल टूल्स, डेटा विश्लेषण और नई शिक्षण तकनीकों में दक्ष होना होगा। पाठ्यक्रम में कोडिंग, लॉजिकल थिंकिंग, नवाचार और साइबर सुरक्षा जैसी क्षमताएँ जोड़कर विद्यार्थियों को 21वीं सदी के ज्ञान-आधारित समाज के लिए तैयार किया जा सकता है।
इसके अलावा, मैं शिक्षकों का सम्मान और सतत प्रशिक्षण को पांचवी चुनौती के रूप में देखता हूं। शिक्षा की गुणवत्ता तभी बढ़ सकती है जब शिक्षक को पर्याप्त संसाधन, आधुनिक साधन, निरंतर प्रशिक्षण और पेशेवर विकास के अवसर मिलें। इसके साथ ही उन्हें उचित सामाजिक सम्मान और सुरक्षित कार्य वातावरण भी प्रदान किया जाना चाहिए।
सरकार को कार्यशालाएँ, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और कौशल-विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को नई तकनीक और नवाचारपूर्ण शिक्षण विधियों में दक्ष बनाना चाहिए।
यदि शिक्षक का मनोबल ऊँचा होगा, उनका जीवन स्तर संतुलित और सम्मानित होगा, तो वे न केवल ज्ञान का संचार करेंगे, बल्कि बच्चों के चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों और रचनात्मकता को भी नई दिशा देंगे। इस प्रकार, शिक्षक को सशक्त और सम्मानित बनाना ही शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है।
साथियो,
हम अमृत काल में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, नैतिक और वैज्ञानिक विकास भी हमारा उद्देश्य है। शिक्षा का लक्ष्य केवल रोजगार तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों को स्वावलंबी, नवाचारी और संवेदनशील नागरिक बनाना होना चाहिए।
मैं समझता हूं कि शिक्षक इस परिवर्तन के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। वे ऐसे नागरिक तैयार करें जो न केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता के लिए काम करें, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए उत्तरदायी हों। 2047 तक की शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान और नवाचार का मुख्य स्थान होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि भारत का नाम वैश्विक स्तर पर ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बने।
मेरा मानना है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं में आत्मनिर्भरता के महत्व को गहराई से स्थापित करना आवश्यक है। इसके लिए हमें उन्हें प्रेरित कर स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा और अनावश्यक विदेशी ब्रांड पर निर्भरता को कम करना होगा। ऐसा करने से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी।
यदि हमें 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करना है तो हमें यह समझना होगा, “यथा शिक्षक तथा राष्ट्र।” यदि हमारे शिक्षक सशक्त और प्रेरक हैं तो हमारे विद्यार्थी भी सशक्त होंगे, और यदि विद्यार्थी सशक्त हैं तो राष्ट्र निश्चित ही महान बनेगा।
अंत में मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए ‘संयुक्त शिक्षक संघ’ को साधुवाद देता हूं। आइए, हम संकल्प लें कि हम विद्यार्थियों को सोचने, सीखने और नेतृत्व करने की क्षमता देंगे। और हम मिलकर 2047 तक भारत को एक विकसित, समृद्ध और संस्कारयुक्त राष्ट्र बनाएँगे।
धन्यवाद,
जय हिंद!