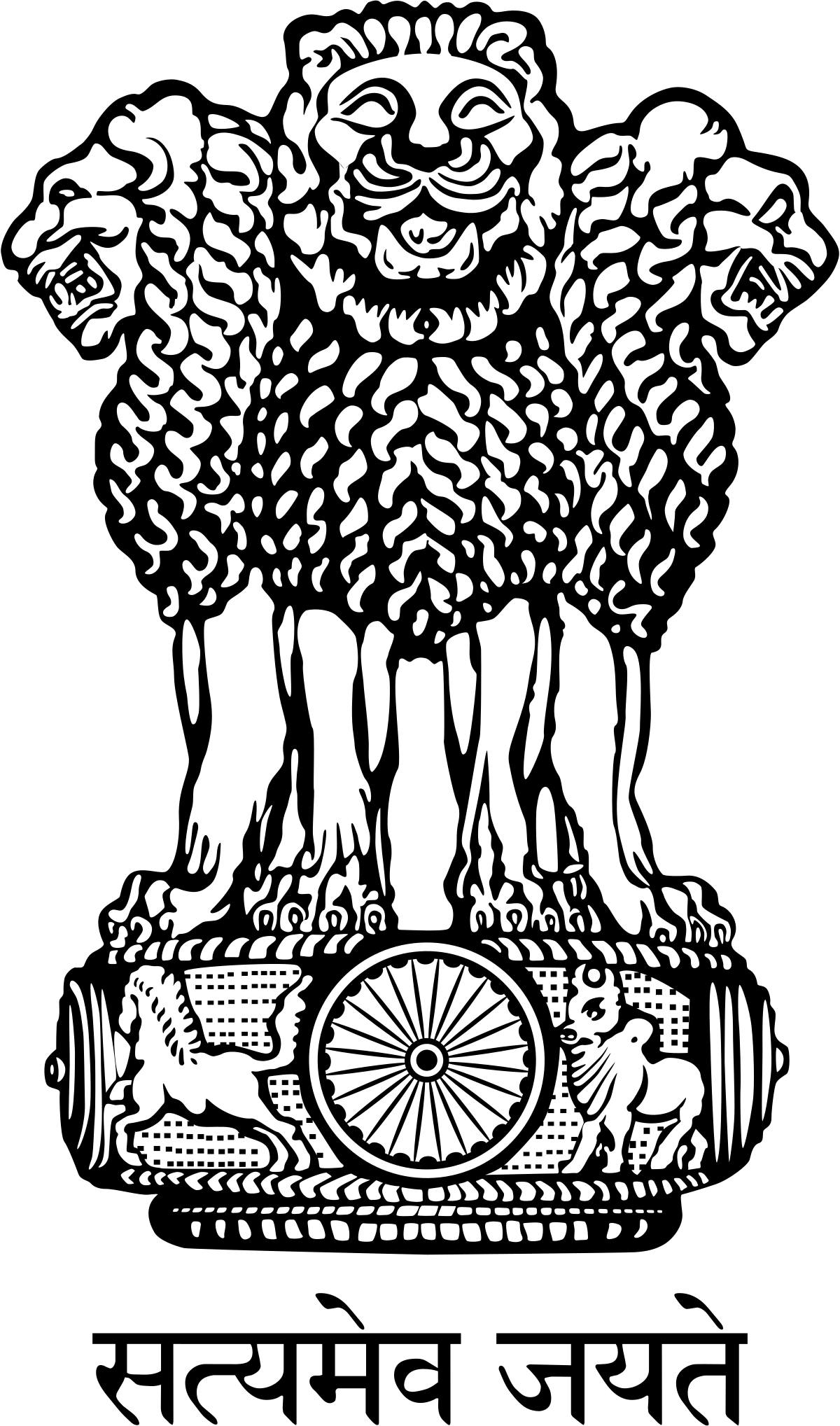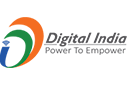SPEECH OF HON’BLE GOVERNOR PUNJAB AND ADMINISTRATOR, UT CHANDIGARH, SHRI GULAB CHAND KATARIA AT THE 11TH All INDIA CONFERENCE OF LINGUISTICS AND FOLKLORE HELD AT DR. MANMOHAN SINGH AUDITORIUM, PUNJAB AGRICULTURAL UNIVERSITY (PAU), LUDHIANA, ON OCTOBER 10
- by Admin
- 2025-10-10 14:05
11वें अखिल भारतीय भाषाविज्ञान एवं लोककथा सम्मेलन के अवसर पर राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का संबोधनदिनांकः 10.10.2025, शुक्रवार समयः दोपहर 12:00 बजे स्थानः लुधियाना
नमस्कार!
यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि मैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में आयोजित 11वें अखिल भारतीय भाषाविज्ञान और लोककथा सम्मेलन के इस प्रतिष्ठित समारोह को संबोधित कर रहा हूँ।
मैं, हमारे महान राष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पधारे आप सभी विद्वानों का अभिनंदन करता हूँ। आपकी उपस्थिति केवल भाषाविज्ञान और लोककथाओं के महत्व की पुष्टि ही नहीं करती, बल्कि भारत की अमूर्त विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के हमारे सामूहिक संकल्प को भी मजबूत करती है।
देवियो और सज्जनो,
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, न केवल पंजाब का बल्कि पूरे राष्ट्र का गौरव है। इसकी स्थापना के पश्चात् से ही इसने भारत की कृषि प्रगति में अद्वितीय योगदान दिया है। हरित क्रांति के ऐतिहासिक दौर में इस विश्वविद्यालय ने उच्च उत्पादकता वाली गेहूँ और धान की किस्मों को विकसित कर पंजाब को “देश का अन्न भंडार” बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह उपलब्धि केवल पंजाब तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हुई।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। वर्तमान में यह संस्थान अपने 6 कॉलेजों में 32 विभागों और 3 स्कूलों के माध्यम से, लुधियाना और बाहरी स्थानों पर 11 स्नातक प्रोग्रामों के अलावा 43 मास्टर और 29 पीएचडी प्रोग्राम प्रदान करता है।
गर्व का विषय है कि आज तक इस विश्वविद्यालय ने 900 से अधिक किस्में विकसित की हैं, जिनमें गेहूँ, धान, मक्का, दलहन, तिलहन, फल एवं सब्ज़ियों सहित विविध फसलों की किस्में शामिल हैं। ये उपलब्धियाँ किसानों की आय वृद्धि और राष्ट्र की समृद्धि में निरंतर योगदान दे रही हैं। विश्वविद्यालय की विस्तार सेवाएँ, किसान मेले, प्रशिक्षण शिविर और तकनीकी मार्गदर्शन ने खेत और प्रयोगशाला के बीच की दूरी को पाटने का कार्य किया है।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय केवल कृषि अनुसंधान और तकनीकी नवाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावी पीढ़ी के कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को भी तैयार कर रहा है। इस संस्थान से शिक्षित विद्यार्थी देश-विदेश में कृषि के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं।
आज जब जलवायु परिवर्तन, जल संकट, मिट्टी की सेहत और फसल विविधीकरण जैसी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, तब यह विश्वविद्यालय किसानों को पानी बचाने वाली तकनीकों, जैविक खेती और स्मार्ट कृषि की दिशा में मार्गदर्शन दे रहा है। इस प्रकार यह केवल वर्तमान ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी कृषि व्यवस्था का निर्माण कर रहा है।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना से ही कृषि अनुसंधान और विस्तार कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त की है। किंतु आज का अवसर विशेष है क्योंकि यह संस्था, जो राष्ट्र को अन्न प्रदान करने के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है, आज भाषा, लोककथा और स्वदेशी ज्ञान पर संवाद का मंच बनी है। वास्तव में, जैसे हमारी मिट्टी में फसलें पल्लवित होती हैं, वैसे ही हमारी परंपराओं में ज्ञान का पुष्पन होता है। दोनों ही मानव सभ्यता को पोषण देते हैं।
देवियो और सज्जनो,
विश्वविद्यालय के ‘कृषि पत्रकारिता, भाषा एवं संस्कृति विभाग’ और ‘डॉ. सुरजीत पातर चेयर’ द्वारा इस 11वें अखिल भारतीय भाषाविज्ञान और लोककथा सम्मेलन का आयोजन एक सराहनीय पहल है। 8 से 10 अक्टूबर 2025 तक आयोजित यह सम्मेलन अपने दायरे और महत्व दोनों में अद्वितीय है।
भाषाविज्ञान का तात्पर्य भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो यह समझने में मदद करता है कि समाज किस प्रकार सोचता है, संवाद करता है और ज्ञान को संरक्षित करता है। दूसरी ओर, लोककथा जीवित परंपराओं, मौखिक इतिहास, गीतों, कहावतों और अनुष्ठानों का भंडार है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और मूल्यों को स्थानांतरित करता है। ये दोनों ही अनुशासन सांस्कृतिक स्मृति के स्तंभ हैं।
तकनीकी प्रगति के इस युग में, हमें यह सोचना होगा कि हमें एक सभ्यता के रूप में क्या स्थिर बनाए रखता है। इसका उत्तर है, भाषा, लोककथा और स्वदेशी ज्ञान। यही हमें जड़ों से जोड़ते हैं और आकाश की ओर उड़ान भरने की शक्ति देते हैं।
देवियो और सज्जनो,
भारत विश्व की सबसे बड़ी भाषाई प्रयोगशाला है, जहां 22 आधिकारिक भाषाएँ और 19,500 से अधिक बोलियाँ बोली जाती हैं जो इसे दुनिया का सबसे बहुभाषी देश बनाती हैं। यहाँ हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर न केवल भाषा, बल्कि उसका लहजा, शब्दावली, मुहावरे और कहावतें भी बदल जाती हैं। यही भाषाई विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर है। यह हमें सिखाती है कि भारत की आत्मा किसी एक भाषा या परंपरा में नहीं, बल्कि सबके सुंदर संगम में बसती है।
भाषाएँ संवाद का साधन होने सहित भावनाओं, अनुभवों और इतिहास की जीवित अभिव्यक्तियाँ हैं, जो लोककथाओं, लोकगीतों और परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के मूल्यों को आगे बढ़ाती हैं।
इसलिए, जब हम भारतीय भाषाओं और लोककथाओं पर चर्चा करते हैं, तो वास्तव में हम भारत की आत्मा से संवाद कर रहे होते हैं, उस आत्मा से, जो विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है।
भारत की विशाल व विविध संस्कृति की तरह उसकी लोककथाएँ भी जीवंत, प्रेरणादायक और लोकजीवन की सजीव अभिव्यक्तियाँ हैं। भारत की लोककथा परंपरा अत्यंत प्राचीन है। पंचतंत्र, जातक कथाएँ, हितोपदेश, बेताल पच्चीसी और कथासरित्सागर जैसी रचनाएँ भारतीय ज्ञान और संवेदना का प्रतीक हैं।
पंजाब की हीर-रांझा, सोहनी-महीवाल, पूरण भगत और मिर्जा-साहिबा जैसी कथाएँ केवल प्रेम की कहानियाँ नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और सामाजिक न्याय की प्रतीक हैं। लोककथाओं में भावनाओं की गहराई और लोकबुद्धि की सरलता दोनों विद्यमान हैं, और यही कारण है कि वे आज भी समय और सीमाओं से परे होकर जनमानस में जीवित हैं।
आज के युवाओं के लिए लोककथाएँ केवल अतीत की कहानियाँ नहीं हैं, वे मूल्यों की पुनर्खोज का माध्यम हैं। जब युवा पीढ़ी लोककथाओं से जुड़ती है, तो उसमें अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ रचनात्मक सोच की प्रेरणा भी मिलती है।
हमें चाहिए कि हम लोकभाषाओं और लोककथाओं को डिजिटल माध्यमों, एनिमेशन फिल्मों, स्कूल पाठ्यक्रमों, और सामुदायिक परियोजनाओं के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचाएँ। इससे हमारी परंपरा जीवित रहेगी और युवाओं को अपनी जड़ों पर गर्व भी होगा।
देवियो और सज्जनो,
आज जब वैश्वीकरण और तकनीकी युग ने भाषाई सीमाओं को लगभग मिटा दिया है, तब लोकभाषाओं और बोलियों का संरक्षण एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब कोई भाषा लुप्त होती है, तो केवल शब्द नहीं मिटते, एक पूरी संस्कृति, एक सोच और एक इतिहास समाप्त हो जाता है।
इसलिए, हमें ऐसे शैक्षणिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो स्थानीय भाषाओं में अनुसंधान, शिक्षा और सृजन को बढ़ावा दें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी मातृभाषा आधारित शिक्षा पर जो ज़ोर दिया है, वह इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा प्राप्त की है। दशकों तक हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर चर्चा करते रहे हैं, जो अक्सर समाज की वास्तविकताओं से कटी हुई थी। उसमें रटने की प्रवृत्ति, परीक्षा परिणामों की संकीर्णता और ज्ञान की सीमित परिभाषा को प्राथमिकता दी जाती रही। स्वदेशी परंपराएँ, स्थानीय भाषाएँ और सामुदायिक ज्ञान को या तो गौण माना गया या हाशिए पर डाल दिया गया।
लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को पूरी तरह बदलने का साहसिक प्रयास किया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार शिक्षा नीति ने मातृभाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और लोक परंपराओं के महत्व को स्वीकार किया है।
यह नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि कक्षा 5 तक और वरीयता से कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए। यह शैक्षणिक सुधार और सभ्यतागत पुनर्जागरण है, जिसमें भारतीय अस्मिता व सांस्कृतिक आत्मविश्वास को स्थान दिया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषावाद पर विशेष बल देती है। यह अंग्रेज़ी को ज्ञान का एकमात्र द्वार नहीं मानती और न ही संस्कृत, तमिल, पंजाबी, उड़िया या जनजातीय भाषाओं को हाशिए पर छोड़ती है। इसके बजाय यह प्रत्येक विद्यार्थी को बहुभाषी बनने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि भारत की भाषाई विविधता उसकी शक्ति बन सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उचित ही कहा है कि भारत की भाषाई विविधता चुनौती नहीं, बल्कि हमारी अनमोल धरोहर है।
यह नीति केवल भाषाओं तक सीमित नहीं है। यह सोच और दृष्टि में बदलाव लाने का आह्वान करती है। इसमें कौशल आधारित शिक्षा, तकनीक का उपयोग, शोध और नवाचार पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम न रहकर, जीवन और समाज को समृद्ध बनाने का साधन बने।
साथ ही, यह नीति ‘‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’’ की संकल्पना को भी मजबूत करती है। जब एक बच्चा अपनी मातृभाषा में ज्ञान अर्जित करता है और साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं को सीखता है, तो उसमें न केवल आत्मविश्वास विकसित होता है बल्कि वह विविधता में एकता की भारतीय अवधारणा को भी गहराई से अनुभव करता है।
इस प्रकार, मोदी जी की दृष्टि में शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रनिर्माण का आधार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी दृष्टि का ठोस प्रतिबिंब है। यह नीति भारत को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और विश्व को दिशा देने वाला ज्ञान-समाज बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
माननीय विद्वानो, मित्रो और छात्रो,
पिछले दो दिनों में आपने भाषाविज्ञान और लोककथा के विषय पर गहन विचार-विमर्श किया। यह स्मरण रहे कि आपकी ज़िम्मेदारी केवल अकादमिक जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज तक भी विस्तृत है। आपके शोध-पत्र, चर्चाएँ और अनुशंसाएँ एक मजबूत, विवेकशील और समावेशी भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगी।
एक भारतीय होने के नाते मुझे और भी गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत पुनः एक ज्ञान-सभ्यता के रूप में उभर रहा है, जहाँ आधुनिक शिक्षा और लोककथा साथ-साथ चलती हैं, जहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान स्वदेशी ज्ञान के प्रति सम्मान प्रकट करता है और जहाँ प्रत्येक बच्चा केवल पाठ्यपुस्तकों से नहीं बल्कि अपनी लोक कहानियों से भी सीखता है।
अंत में, हम सब मिलकर यही संकल्प लें कि अपनी मातृभाषा, लोक गीत, कथाएँ, बोलियाँ और साहित्य, इन सबको संजोकर अगली पीढ़ी को वह आत्मबल दें, जिससे वे वैश्विक मंच पर भारतीय अस्मिता का डंका बजा सकें। यही इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है; यही हमारी आगे की यात्रा की प्रेरणा है।
आइए इस सम्मेलन को उस यात्रा का एक मील का पत्थर बनाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को आगे बढ़ाएं। हर आवाज़, हर भाषा और हर कहानी को हमारी राष्ट्रीय धारा में शामिल करें।
धन्यवाद,
जय हिंद!