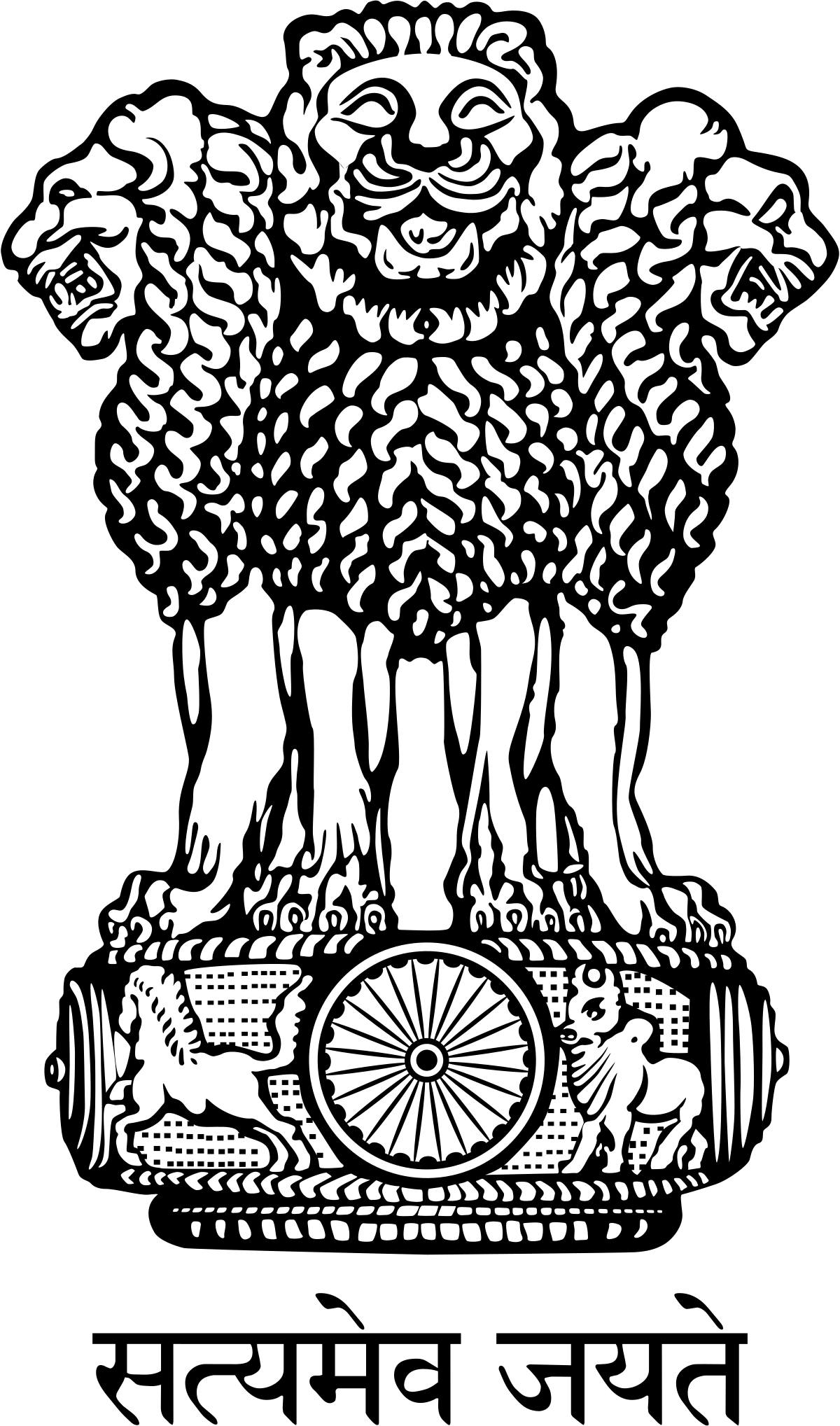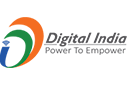SPEECH OF PUNJAB GOVERNOR AND ADMINISTRATOR, UT CHANDIGARH, SHRI GULAB CHAND KATARIA ON THE OCCASION OF COMMEMORATION OF 150 YEARS OF VANDE MATARAM AT CHANDIGARH ON NOVEMBER 7, 2025.
- by Admin
- 2025-11-07 12:05
राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का संबोधनदिनांकः 07.11.2025, शुक्रवार समयः सुबह 10:00 बजे स्थानः चंडीगढ़
नमस्कार!
आज इस पावन अवसर पर आप सबके साथ “वंदे मातरम्” के 150 वर्षों के इस ऐतिहासिक उत्सव में सम्मिलित होकर मेरा हृदय गर्व और आनंद से भर गया है। “वंदे मातरम्” एक ऐसा गीत है, जो समय की सीमाओं से परे है। यह केवल शब्दों और संगीत का संयोजन नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र की धड़कन और उसकी आत्मा की वाणी है।
“वंदे मातरम्” की रचना महान विचारक बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1875 में किया था और इसे उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ में वर्ष 1882 में प्रकाशित किया। इस अद्भुत रचना ने भारत की आत्मा को स्वर दिया, ऐसी मातृभूमि की भावना को, जो केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान और करुणा का सजीव प्रतीक है। विश्व के साहित्य में बहुत कम ऐसी रचनाएँ हैं, जिनमें सम्पूर्ण राष्ट्र की चेतना को जागृत करने की इतनी अपूर्व क्षमता हो।
“वंदे मातरम्” की रचना करने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 1838 में बंगाल के 24 परगना ज़िले के कांतलपाड़ा गाँव में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और ब्रिटिश प्रशासन में डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया। लेकिन सरकारी सेवा के साथ-साथ उन्होंने अपने लेखन को राष्ट्रसेवा का माध्यम बनाया। उनकी रचनाएँ-दुर्गेशनंदिनी, कपालकुंडला, मृणालिनी और आनंदमठ-सिर्फ साहित्य नहीं, बल्कि भारतीय समाज में देशभक्ति, एकता और आत्मसम्मान की भावना जगाने वाले आंदोलन थे। उनका राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि गहराई से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक था।
उन्होंने “वंदे मातरम्” के माध्यम से भारतभूमि को सिर्फ भूमि नहीं, बल्कि माँ के रूप में देखा। बंकिमचंद्र ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज में स्वाभिमान, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अलख जगाई। सचमुच, वे भारत के उन महापुरुषों में से थे, जिन्होंने शब्दों को जनजागरण का शस्त्र बनाया।
‘वंदे मातरम्’ की विशेषता है कि इसके दो प्रथम पद संस्कृत में और शेष बांग्ला में हैं। यह शैली बंगाल नवजागरण के समय की विशेष सांस्कृतिक विशेषता को इंगित करती है, जब बांग्ला नवजागरण तथा पुरातन शास्त्रीय परंपरा का संगम हुआ। संस्कृत के प्रयोग ने इसे अखिलभारतीय पहचान दिलाई, जबकि बांग्ला के मिश्रण ने उसे लोकजीवन से जोड़ दिया।
देवियो और सज्जनो
“वंदे मातरम्” का गीत सर्वप्रथम गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से गाया गया था। उस ऐतिहासिक क्षण से “वंदे मातरम्” एक गीत भर नहीं रहा, यह स्वतंत्रता आंदोलन का प्राण बन गया, एक ऐसी पुकार जिसने करोड़ों भारतीयों को विदेशी शासन के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया।
“वंदे मातरम्” अर्थात् “माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ”, इन शब्दों में मातृभूमि के प्रति गहन श्रद्धा और भक्ति निहित है। यह वही भूमि है जो हमें पोषित करती है, वही नदियाँ हैं जो हमें जीवन देती हैं, और वही संस्कृति है जो हमारे संस्कारों को आकार देती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में यही शब्द ऐसे सूत्र बने जिन्होंने धर्म, क्षेत्र और भाषा की सीमाओं को पार करते हुए समस्त भारतवासियों को एकता के सूत्र में पिरो दिया। इस गीत ने हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व को स्वर दिया और सभी को भारत माता की मुक्ति के उद्देश्य के लिए प्रेरित किया।
जब स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी, तो “वंदे मातरम्” हमारे क्रांतिकारियों का जयघोष बन गया। इसके उच्चारण से देशभक्तों के हृदय साहस और संकल्प से भर उठते थे। ब्रिटिश शासन ने इसके प्रभाव को भलीभाँति समझा और इसकी सार्वजनिक गायन पर कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिया। परंतु इन प्रतिबंधों से इसकी लौ मंद नहीं पड़ी। देशभक्तों, विद्यार्थियों और सामान्य नागरिकों ने इसे एक प्रतिरोध के रूप में, भारत के भाग्य में अटूट आस्था के प्रतीक के रूप में, निर्भीक होकर गाना और कहना जारी रखा।
1905 के बंग-भंग आंदोलन से लेकर 1938 के गुलबर्गा वंदे मातरम् आंदोलन तक यह गीत एकजुटता और विरोध का प्रतीक बना रहा। जेलों में, आंदोलनों में, और फाँसी के तख्तों पर भी इसके शब्द गूंजते रहे। इसने उन लोगों के मनोबल को सशक्त किया जिन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वप्न के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। “वंदे मातरम्” के प्रत्येक उद्घोष ने यह स्मरण दिलाया कि भारत की आत्मा को कभी बाँधा नहीं जा सकता।
दार्शनिकों और आध्यात्मिक नेताओं ने भी इस गीत की गहराई को समझा। श्री अरविन्दो ने “वंदे मातरम्” को एक आध्यात्मिक मंत्र कहा और इस पवित्र आह्वान ने राष्ट्र की अंतःशक्ति और चेतना को जागृत किया। यह केवल एक देशभक्ति नारा नहीं था, बल्कि एक प्रार्थना थी, एक साधना थी, मातृभूमि के प्रति प्रेम का दैवीय भाव था। इसका प्रभाव राजनीति से कहीं आगे बढ़कर साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति तक फैल गया।
देवियो और सज्जनो
वर्ष 1948-50 दौरान संविधान सभा में राष्ट्रगीत के चयन पर लंबी बहस हुई। कुछ सदस्य वंदे मातरम् को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे, जबकि अन्य ने उसमें धार्मिक प्रतीकों के कारण आपत्ति जताई।
अंततः 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन राष्ट्रगान होगा, पर वंदे मातरम् को भी समान सम्मान दिया जाएगा क्योंकि उसने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इस अमर गीत की प्रथम दो पंक्तियाँ बाद में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत की गईं, जो इसके अमर स्थान का प्रमाण है।
आज जब हम “वंदे मातरम्” के 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तो यह केवल एक ऐतिहासिक अवसर का उत्सव नहीं है, यह भारत की उस सनातन भावना का उत्सव है जो युगों-युगों तक अटूट रही है।
भारत सरकार ने इस महत्त्वपूर्ण अवसर के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आरंभ किया है, जिससे विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों को इस गीत की मूल भावना और इसके क्रांतिकारी संदेश से जोड़ा जा सके। देशभर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ, संगीत समारोह और शैक्षिक अभियान आयोजित किए जा रहे हैं, जो एकता, समर्पण और देशभक्ति के इस अमर संदेश को जन-जन तक पहुँचा रहे हैं।
यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारी युवा पीढ़ी यह समझे कि “वंदे मातरम्” केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि एक जीवंत धरोहर है। यह हमें हमारे पूर्वजों के बलिदानों की याद दिलाता है और हमें ईमानदारी, करुणा और निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा करने की प्रेरणा देता है। जब भी हम “वंदे मातरम्” गाते या सुनते हैं, हम एकता की शक्ति, संकल्प के साहस और मातृभूमि के प्रति शुद्ध प्रेम को पुनः अनुभव करते हैं।
देवियो और सज्जनो
“वंदे मातरम्” सिर्फ एक गीत नहीं है, यह भारत की स्वतंत्रता की आवाज़ है, उसकी अटूट सहनशक्ति की धुन है, और उसकी एकता की आत्मा है। यह आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। यह हमें याद दिलाता है कि अपने देश के प्रति हमारा प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
भारत की एकता, अखंडता, समरसता और ‘विविधता में एकता’ के आदर्श इस गीत में निहित है। संसद, विधानसभाएँ, विद्यालय, गाँव, नगर, सेना, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, संचार माध्यम, सोशल मीडिया, हर जगह यह गीत भारतवासियों को उनके साझा परंपरा, गौरव और संकल्प की याद दिलाता है।
साहित्य, रंगमंच, सिनेमा, चित्रकला, वाद्यसंगीत, नृत्य, सभी भारतीय कलात्मक विधाओं ने ‘वंदे मातरम्’ को प्रोत्साहित किया है। लोकगीत, शास्त्रीय गायन, स्कूल प्रतियोगिता, नाटकों, फिल्मों, चित्रों, रेखांकनों, डाक टिकिटों, स्मारक सिक्कों, सबमें इसका प्रयोग होता रहा है।
आज जब ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पूर्ण हो रहे हैं, यह हमारा दायित्व बनता है कि हम इसके ऐतिहासिक योगदान, सांस्कृतिक महत्व, संवैधानिक स्थान, सामाजिक विमर्श, और प्रेरणास्रोत रूप का संपूर्ण आकलन करें। यह गीत केवल किसी एक धर्म, क्षेत्र या भाषा का नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत का सामूहिक आख्यान और भारतभूमि के गर्व, सम्मान, और दायित्व का उद्घोष है।
‘वंदे मातरम्’ न केवल भारत का राष्ट्रगीत है, बल्कि यह भारत की गैर-राजनीतिक, भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मा का शाश्वत मंत्र है। इसके 150 वर्षों का यह सफर, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना स्वतंत्रता संग्राम के दौर में था। हर भारतीय इसके उच्चारण से देशभक्ति, एकता, आत्मबल, और समर्पण के उद्गार पाता है। यही इसकी चिरस्थायित्व और कालजयी प्रेरणा है।
आज जब राष्ट्र ‘विकसित भारत’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो यह गीत हमें स्मरण कराता है कि सच्चा विकास तभी संभव है जब हम अपनी संस्कृति, एकता और कर्तव्यनिष्ठा को साथ लेकर चलें। “माँ भारती” के प्रति समर्पण, परिश्रम और नवाचार की भावना ही इस गीत का सार है और यही भावना हमें 2047 तक एक विकसित, सशक्त और आत्मविश्वासी भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर करती है।
जब हम इस ऐतिहासिक पड़ाव का उत्सव मना रहे हैं, तो आइए हम अपने पूर्वजों के आदर्शों के प्रति स्वयं को फिर से समर्पित करें। आइए, उस सौहार्द और एकजुटता की भावना को पोषित करें, जिसका प्रतीक “वंदे मातरम्” है; और यह सुनिश्चित करें कि इसका अमर संदेश आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहे, हम सबको देशभक्ति और गर्व के अटूट बंधन में जोड़े रखे।
धन्यवाद,
वंदे मातरम्!
जय हिंद!